शिक्षा इंसान के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में है। रोटी ,कपड़ा और मकान की मूल आवश्यकताओं के बाद मनुष्य जीवन में ऊचाईयों की और बढ़ना चाहता है। इसके लिए तथा पृथ्वी पर भरे हुए रहस्यों को समझने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा समाज की दिशा तथा दशा का निर्धारण करती है कहा जाता है कि अगर किसी देश तथा समाज में बड़े परिवर्तन करने हो तो शिक्षा में समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है। शिक्षा को यही दिशा देने के लिए शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और समय समय पर इन नीतियों में परिवर्तन किया जाता रहा जो की समय की जरुरत थी।
२०२० की नयी शिक्षा नीति को सरकार की बैठक में मंजूरी दे दी गयी है। इसके पहले इसका प्रारूप बनाने के लिए कभी अनुसंधान और प्रयत्न हुए। यह स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है इससे पहले 1968 तथा 1986 में शिक्षा नीतियां लागू की गई थी. 1986 के बाद इस शिक्षा नीति को आने में 34 वर्ष लग गए जिसमें आगामी समय के उद्देश्य तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है वर्तमान में तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य तथा सामाजिक संरचना में होते आमूलचूल परिवर्तनों के मद्देनजर प्रत्येक 10 वर्ष में शिक्षा नीति की समीक्षा तथा आवश्यक बदलाव करने चाहिए. शिक्षा नीति को सरकार एक खास सोच के अंतर्गत तैयार करती है और इसके पीछे कई लोगों की सोच होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के आम चुनाव में अपना चुनावी वादा शिक्षा नीति में परिवर्तन भी रखा था. जून 2017 में इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 11 सदस्य कमेटी का गठन किया गया था, जिसने मई 2019 में शिक्षा नीति से संबंधित प्रारूप तैयार किया नई शिक्षा नीति 2020 की परामर्श प्रक्रिया विश्व की सबसे बड़ी परामर्श प्रक्रिया रही यह जनवरी 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक व्यापक स्तर पर सभी पहलुओं को सम्मिलित करते हुए चर्चा की गई तथा सुझाव लिए गए. 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति के प्रारूप को पेश किया और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गयी।
नयी शिक्षा नीति में कई खास बातें नीचे दिए गए:
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
एनईपी 2020 (NEP 2020) स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है, अब 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू होगा। वहीं स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा पद्धति भी लागू होगी ।
इस शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि केंद्र तथा राज्य के बीच टकराव की स्थिति में दोनों आम सहमति से निर्णय लेंगे।
नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए एग्जाम के साथ-साथ डेमो तथा साक्षात्कार का भी प्रावधान किया गया।
इस शिक्षा नीति में शिक्षकों के स्थानांतरण संबंधित मुख्य प्रावधान किया गया है जिसमें शिक्षकों का स्थानांतरण पर लगभग रोक लग जाएगी और पदोन्नति के समय ही स्थानांतरण किया जा सकेगा इस प्रावधान को शामिल करने का प्रमुख उद्देश्य दुर्गम तथा कम सुविधाओं वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की समस्या से निजात पाना है।
आमतौर पर देखा गया है की ऐसी जगहों पर नियुक्त होने वाले अध्यापक गण अपना स्थानांतरण करवाने को इच्छुक रहते हैं तथा वे क्षेत्र लगातार शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रह जाते हैं। इस नीति से संबंधित दूसरा प्रमुख मुद्दा मातृभाषा को लेकर है, पहले की शिक्षा नीतियों में भी मातृभाषा पर बल देने की बात कही गई थी। लेकिन धरातल पर क्रियान्वित नहीं हो पाई तो सवाल यह है कि क्या नवीन शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान के अनुरूप मातृभाषा को बढ़ावा देने में सफल हो पाएंगे। इसका कारण मातृ भाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का ना होना भी है। कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि आगे चलकर जब विद्यार्थियों को प्रतियोगिताएं में भाग लेने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना ही होगा तो मातृभाषा कहां तक उपयोगी है।
भारत में भाषाई आधार पर स्वतंत्रता के बाद से ही विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं. नवीन शिक्षा नीति के जारी होते ही तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के कुछ संगठनों ने उन पर हिंदी थोपे जाने के आरोप लगाएं परंतु उल्लेखनीय है. कि इस नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है. इसके अंतर्गत त्रिभाषा पैटर्न में अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ संस्कृत तथा तमिल भाषाओं तथा क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा.
बहस का तो कोई अंत नहीं है ,परंतु नवीन शिक्षा नीति शिक्षा के भारतीय करण तथा बदलते समय के अनुसार ज्ञान कौशल तथा मूल्यों का सामंजस्य स्थापित करने में अहम भूमिका अदा करेगी। वर्तमान में शिक्षा जगत से जुड़ी प्रमुख समस्याओं में शिक्षकों की कमी विद्यालयों की कमी कमी शिक्षा सुधार कार्यक्रमों का सफल ना हो पाना ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता में कमी का होना उच्च शिक्षा में प्रोफेसर की जवाबदेही व प्रदर्शन का फार्मूला निर्धारित ना होना तथा विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में कम संख्या में भारतीय विश्वविद्यालयों का शामिल होना यह सब कारण है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े परिवर्तन की गुंजाइश को दर्शाते हैं तथा नवीन शिक्षा नीति इस दिशा में सराहनीय कदम है.
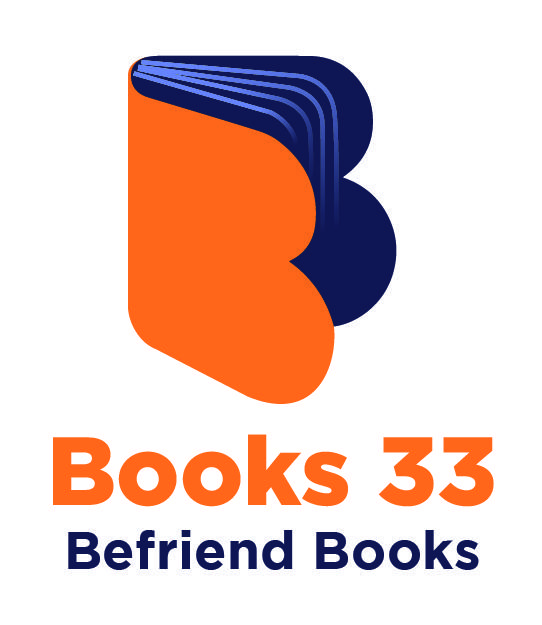
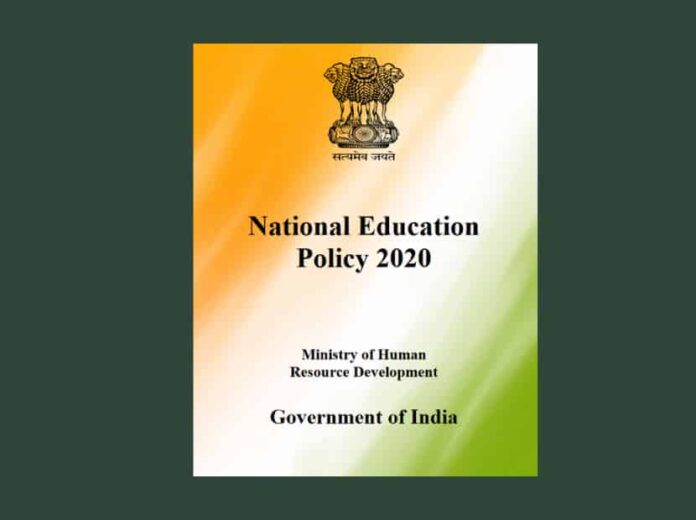
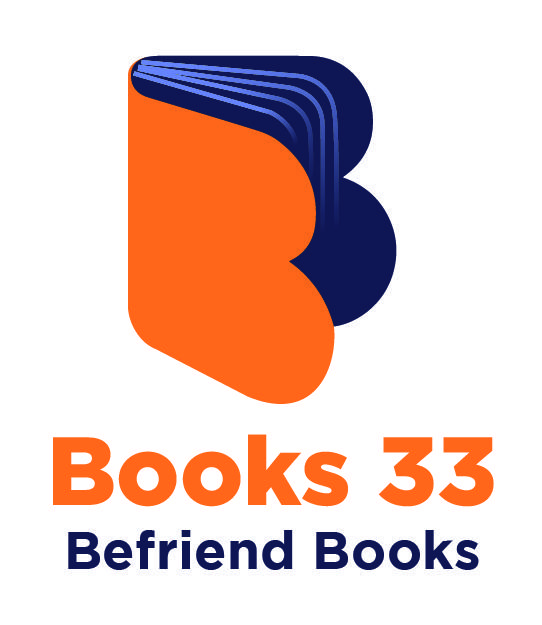

 Each title in our collection is more than just a book - it’s a ‘green gift’, promoting mindful reading, sustainable values, and a culture of eco-conscious living. By gifting books, you open doors to new ideas, support lifelong learning, and nurture a more informed, compassionate, and environmentally aware individual.
Each title in our collection is more than just a book - it’s a ‘green gift’, promoting mindful reading, sustainable values, and a culture of eco-conscious living. By gifting books, you open doors to new ideas, support lifelong learning, and nurture a more informed, compassionate, and environmentally aware individual.
An interesting article.